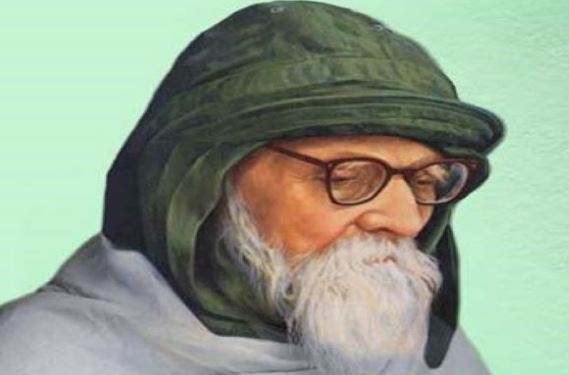कभी कभी कुछ चीजें हमारे ज़हन में बचपन से बैठ जाती है। ये अच्छा है , वो ख़राब है, वो ठीक है, ये ग़लत है, वो हमारे दोस्त है और ये दुश्मन है। बचपन में हमारे दिमाग़ में डाली वो बातें हमें हमेशा सच ही लगती है और बड़े होने के बाद वही बातें हमारे लिए यथार्थ की वो धरातल होती है जिसपर हम अपने सोच की फ़सल को लगाते हैं। अब अगर वो धरातल हमारे नुमाइंदों की हो तो शायद नयी सोच की सारी फ़सल भी उसी चश्मे से देखी जायेगी। यह मुग़ल बनाम हम भी शायद उसी धरातल से उपजी फ़सल है जिसे हम सियासत की बाज़ार में हर दिन ख़रीद और बेच रहे हैं।
किसी जमाने में मैं ने बंकिमचंद्र चैटर्जी की महान रचना आनंद मठ पढ़ा था। अब वो बचपन के दिन थे इसलिए मुझे किताब में लिखे अक्षर तो समझ में आ गए थे परंतु किताब की भीतर का छुपे भाव को शायद नहीं समझ पाया। बड़े होने पर गुरुओं ने आनंद मठ का महत्व मुझे राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी समझाया जिसमें उस समय के बंगाल में मुस्लिम शासकों का पतन, समाज के नैतिक चरित्र की गिरावट, सन्यासी विद्रोह और अंग्रेज़ी साम्राज्य की दस्तक सभी शामिल थे।